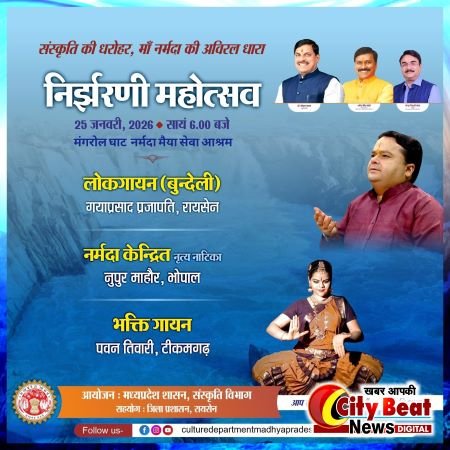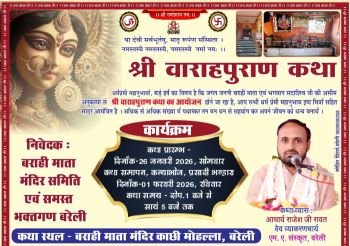भारत जैसे विशाल और विविध देश में डिजिटल प्रगति की रफ्तार अत्यंत महत्वाकांक्षी रही है। शहरों में तेज इंटरनेट, स्टार्टअप्स और स्मार्ट इनोवेशन की गूंज है, लेकिन दूसरी ओर, ग्रामीण इलाकों में अब भी एक स्थिर इंटरनेट कनेक्शन का इंतजार है — जो आज की दुनिया में एक डिजिटल जीवनरेखा बन चुका है।
### बिखरा हुआ डिजिटल नक्शा
भारत में भले ही मोबाइल यूजर्स की संख्या एक अरब से अधिक हो, लेकिन ये आंकड़े हकीकत की गहराई को नहीं दर्शाते। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 37% लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 67% तक पहुंच चुका है। यह असमानता दो अलग-अलग भारतों की कहानी कहती है — एक डिजिटल रूप से जुड़ा हुआ, दूसरा अब भी इंतजार में।
### यह दूरी क्यों मायने रखती है?
*शिक्षा पर असर:* महामारी के दौरान जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई, तो ग्रामीण छात्रों के पास न तो डिवाइस थे, न ही इंटरनेट। कई को पढ़ाई छोड़नी पड़ी या वे पीछे रह गए।
*रोज़गार और विकास की रुकावट:* किसान, बुनकर और छोटे व्यापारी डिजिटल टूल्स की मदद से नए बाजारों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इंटरनेट की कमी से यह संभावना सपना बनी हुई है।
*सूचना की शक्ति:* सरकारी योजनाओं से लेकर मौसम की जानकारी तक, इंटरनेट समय पर सूचना पाने का जरिया है। इसके बिना ग्रामीण समुदाय पीछे छूट जाते हैं।
### क्या किया जा रहा है?
2015 में शुरू हुई ‘डिजिटल इंडिया’ मुहिम का मकसद हर गांव को इंटरनेट से जोड़ना था। भारतनेट (BharatNet) प्रोजेक्ट के तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना है। लेकिन 2025 की शुरुआत तक सिर्फ 60% पंचायतें ही कनेक्ट हो पाई हैं।
### चुनौतियाँ क्या हैं?
*इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें:* दुर्गम इलाकों में केबल बिछाना आसान नहीं है — न ही सस्ता।
*महंगा डेटा और डिवाइस:* नेटवर्क आने के बाद भी मोबाइल और डेटा पैक ग्रामीण लोगों की पहुंच से बाहर हैं।
*डिजिटल साक्षरता की कमी:* सिर्फ इंटरनेट होना काफी नहीं, उसे सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना भी ज़रूरी है। इस दिशा में अभी काफी काम बाकी है।
### उम्मीद की किरण
कुछ एनजीओ इस दिशा में शानदार काम कर रहे हैं। ‘डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन’ जैसे संगठन कम्युनिटी इंटरनेट सेंटर बना रहे हैं, जहां लोग इंटरनेट का उपयोग करना सीख रहे हैं — शिक्षा, स्वास्थ्य और कारोबार के लिए।
### साझेदारी में ताकत
सरकार और निजी कंपनियों के बीच सहयोग से यह कार्य तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। टेलीकॉम कंपनियों को प्रोत्साहन देकर वे दूरदराज क्षेत्रों में नेटवर्क बिछा सकती हैं। साथ ही, टेक कंपनियाँ सस्ते डिवाइस और स्थानीय भाषा में सामग्री बनाकर इंटरनेट को और सहज बना सकती हैं।
### निष्कर्ष
अगर भारत को सच में डिजिटल बनना है, तो इंटरनेट केवल शहरी विशेषाधिकार नहीं रह सकता। असली विकास तभी होगा जब कोई भी गांव डिजिटल अंधेरे में न रहे। सही नीति, बेहतर भागीदारी और लोगों को केंद्र में रखकर सोचने से यह दूरी पाटी जा सकती है।
—
*गिग इकोनॉमी का उभार: भारत में अवसर और चुनौतियाँ*
श्रृष्टि चौबे द्वारा
भारत की कार्य संस्कृति धीरे-धीरे बदल रही है। अब जीवनभर एक ही नौकरी करने का दौर बीत रहा है और उसकी जगह ले रहे हैं गिग वर्कर्स — यानी वे लोग जो छोटे-छोटे अस्थायी कार्यों से अपनी आजीविका चला रहे हैं।
### गिग इकोनॉमी क्या है?
यह पारंपरिक 9 से 5 नौकरी का विकल्प है। इसमें व्यक्ति किसी एक नियोक्ता के अधीन नहीं होता, बल्कि ज़रूरत के अनुसार अल्पकालिक कार्य करता है। Uber, Swiggy, Upwork जैसे प्लेटफार्म्स ने यह काम आसान बना दिया है।
### क्यों लोकप्रिय हो रही है?
*लचीलापन:* गिग वर्कर्स को अपने समय और कार्य के तरीके पर ज्यादा नियंत्रण होता है।
*अनेक आमदनी के रास्ते:* एक व्यक्ति एक साथ कई कार्य कर सकता है, जिससे उसकी आमदनी स्थिर सैलरी से अधिक विविध हो जाती है।
*कौशल और बाज़ार का मेल:* चाहे आप लेखक हों या तकनीकी विशेषज्ञ, अब घर बैठे वैश्विक मांग को पूरा कर सकते हैं।
### लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं है
*सुरक्षा का अभाव:* ज़्यादातर गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा, छुट्टियाँ या पेंशन जैसी सुविधाएँ नहीं मिलतीं।
*अनिश्चित आमदनी:* कभी आमदनी अधिक, कभी बेहद कम। इससे वित्तीय योजना मुश्किल हो जाती है।
*कानूनी अस्पष्टता:* श्रम कानून अब भी पारंपरिक नौकरियों पर केंद्रित हैं। इससे गिग वर्कर्स कानूनी दृष्टि से असुरक्षित रह जाते हैं।
### आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व
Boston Consulting Group और Michael & Susan Dell Foundation की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत की गिग इकोनॉमी 90 मिलियन गैर-कृषि नौकरियाँ पैदा कर सकती है और जीडीपी में 1.25% तक की बढ़ोत्तरी ला सकती है। यह सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक संरचनात्मक बदलाव है।
### टिकाऊ भविष्य की राह
*नीतियों में स्पष्टता:* गिग वर्कर्स के अधिकारों को कानूनी रूप से परिभाषित करना ज़रूरी है — जैसे उचित वेतन, विवाद समाधान प्रणाली, और शोषण से सुरक्षा।
*सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:* सरकार और प्लेटफार्म कंपनियाँ मिलकर बीमा, पेंशन और इमरजेंसी फंड जैसी योजनाएं बना सकती हैं।
*कौशल विकास:* ट्रेनिंग प्रोग्राम्स से गिग वर्कर्स केवल कम वेतन वाली नौकरियों में न फंसे रहें, बल्कि समय के साथ विशेषज्ञता हासिल करें।
### व्यापक दृष्टिकोण
गिग इकोनॉमी ने महिलाओं, युवाओं और छोटे शहरों के लोगों को नई राहें दी हैं। लेकिन इसने यह भी दिखाया है कि जब नवाचार, नियमों से आगे निकल जाता है, तो असमानता बढ़ सकती है।
अब आवश्यकता है — संतुलन की। लचीलापन हो, पर गरिमा के साथ। सुविधा हो, पर न्यायसंगत मुआवजे के साथ।
गिग वर्कर्स को केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की रीढ़ मानकर आगे बढ़ना होगा। उनकी भागीदारी को सम्मान देना हमारी आर्थिक संरचना की स्थिरता का आधार बनेगा।
और इसके लिए ज़रूरी है — नीति निर्माताओं, टेक कंपनियों और नागरिक समाज का सहयोग। एक ऐसा सामाजिक अनुबंध बने जो संरक्षण तो दे, लेकिन नियंत्रण न करे। समर्थन दे, लेकिन आत्मनिर्भरता बनाए रखे।
क्योंकि अंततः गिग इकोनॉमी की सफलता केवल उसके आकार में नहीं, बल्कि उसमें समावेशित न्याय में निहित है।
श्रृष्टि चौबे लेखिका के स्वतंत्र विचार …